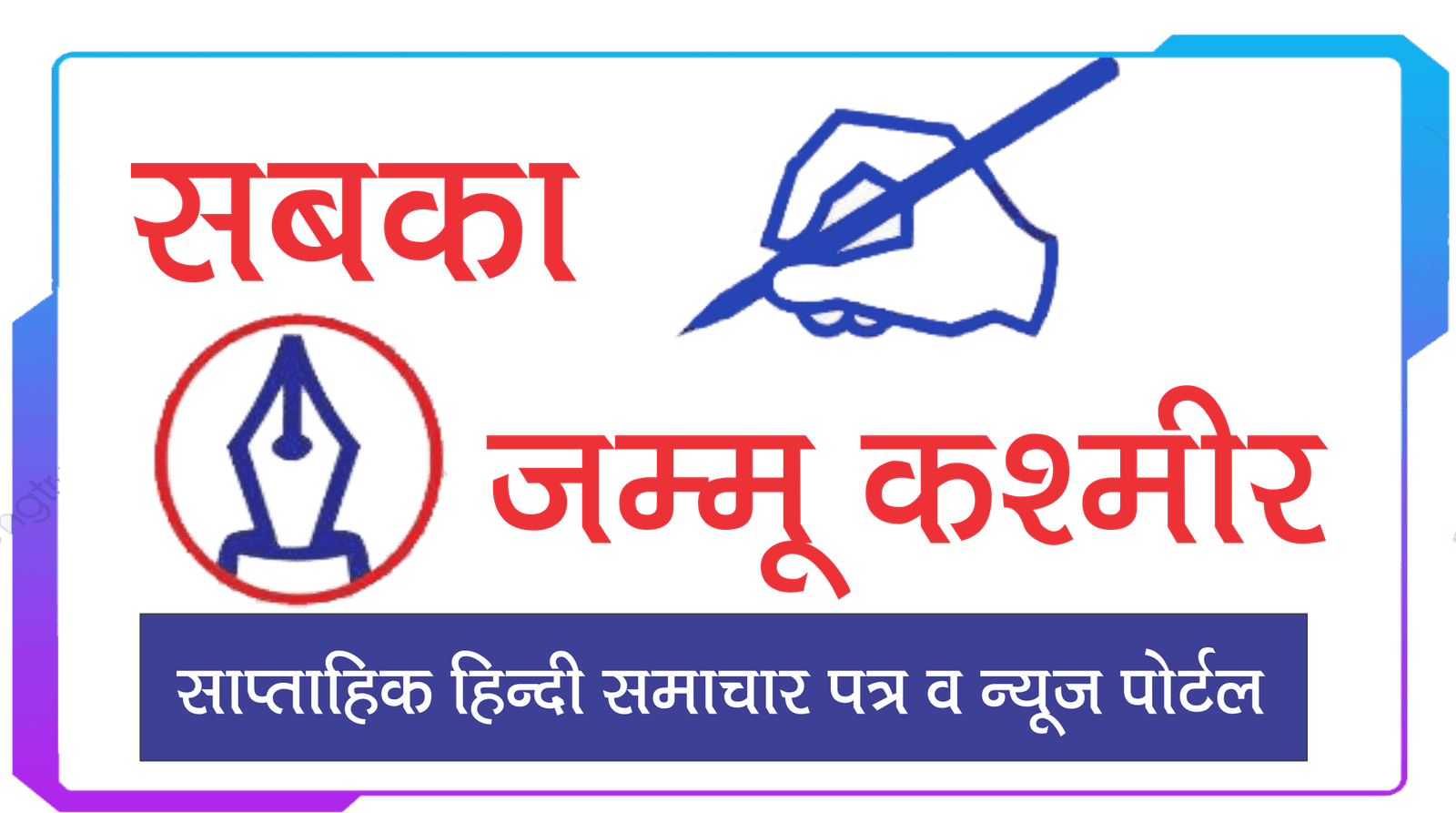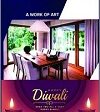जहाँ मज़दूर अदृश्य है!

(आलेख : नंदिता हक्सर, अनुवाद : अंजली देशपांडे)
कई साल पहले, मैं साहित्य उत्सवों के विचार से रोमांचित होती थी और उनमें उत्साही भागीदार हुआ करती थी। मैं अरुंधति रॉय के इस बयान से सहमत नहीं थी कि ये केवल अभिजात वर्गीय उत्सव होते हैं। ऐसे अन्य लेखकों से मिलना, जो खुद उत्पीड़न का मुकाबला कर रहे हों, अनेकानेक देशों और संस्कारों के कवियों को सुनना, और विचारों के आदान-प्रदान का ऐसा अवसर — मुझे तो यह ताज़ी हवा के झोंके-सा लगता था। जो लोग कहीं से भी उच्च मध्यम या बुर्जूवा वर्ग के नहीं हैं, उन्हें भी ऐसे लेखकों से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का मौक़ा भी तो ऐसे उत्सवों में ही मिलता है!
लेकिन जयपुर लिटरेचर फ़ेस्टिवल, अरुंधति रॉय की आलोचना की सच्चाई का सबूत बन गया है। यह एक ऐसा त्योहार है, जो अनेक लेखकों और कवियों को तो आकर्षित करता है, लेकिन इस त्योहार के पाँच दिन अभिजात वर्ग के हित को भी अलग-अलग तरीके से साधते हैं। अन्यथा वेदांता और मारुति सुज़ुकी जैसे कॉर्पोरेट इस महोत्सव को प्रायोजित क्यों करते?
जयपुर साहित्योत्सव की तुलना ठीक ही महाकुंभ से की गयी है। हमारे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में से एक ने जयपुर साहित्योत्सव के बारे में बताया कि “दुनिया भर से 300 से अधिक वक्ता इस महाकुंभ में, जो साहित्य, कला और संगीत… का एक भव्य संगम होगा, देश और दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।”
शायद महाकुंभ का रूपक अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़े धार्मिक उत्सव में हम तमाशा और आडंबर तो देखते हैं, लेकिन अपने समय के ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत के लिए उसमें कोई जगह नहीं होती। वास्तविक दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों से दो-चार होने का इनमें कोई मौक़ा नहीं होता ; ऐसे मुद्दे, जिनसे कई लेखक वास्तव में जुड़े हो सकते हैं।
जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की भी जाती है, तो चर्चा का प्रारूप ही प्रभाव को बहुत कम कर देता है। इसके विपरीत, केरल के कोझिकोड में उत्सव में, बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास ‘प्रोफेट सॉन्ग’ के आयरिश लेखक पॉल लिंच ने बताया कि कैसे उनकी किताब इस विषय पर है कि किस तरह लोग जान कर भी मानने को तैयार नहीं होते कि ‘चीज़ें कितनी ख़राब हालत में हैं, कि सब कुछ खत्म हो चुका होना अब एक तथ्य है।’
तो चीज़ें कितनी ख़राब हालत में हैं?
वेदांता द्वारा पर्यावरण पर पड़नेवाला विनाशकारी प्रभाव और मारुति सुज़ुकी संयंत्रों में मजदूरों के काम के हालात, उस अंधकारमय भविष्य की एक झलक है, जो ग्रामीण और शहरी भारत के मज़दूरों की अगली पीढ़ी का इंतज़ार कर रही है।
मीडिया जयपुर साहित्योत्सव की जमकर तारीफ़ कर रहा है। इसका एक नमूना देखें : “…वेदांता प्रस्तुत करता है, मारुति सुज़ुकी के सहयोग से और विडा द्वारा संचालित, विश्व-स्तर पर किताबों और विचारों के भव्यतम जश्न के रूप में मान्यता प्राप्त जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025, जो आज एक शांत गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ…।”
उद्घाटन समारोह के बारे में पढ़कर मुझे याद आया कि 2012 में यूनियन की माँगों के चार्टर पर मारुति सुज़ुकी प्रबंधन की कैसी प्रतिक्रिया रही थी, जब मज़दूरों का गुस्सा फूट पड़ा था। जापानी प्रबंधन ने यह मानने से इंकार कर दिया था कि मज़दूरों के पास शिकायतों की कोई वजह है ; इसके बजाय उन्होंने विवाद को आपराधिक बना दिया था और पूरी ट्रेड यूनियन को हत्या के मामले में फँसा दिया गया था, जिसमें यूनियन के 13 नेताओं को अंततः आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी गयी। 2,000 से अधिक श्रमिकों को बिना किसी विभागीय जाँच के काम से निकाल दिया गया। प्रबंधन ने मानेसर संयंत्र में “वास्तु मुद्दों” को सुलझाने के लिए बंगलुरु के एक प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी, दैवज्ञ के.एन. सोमयाजी को यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था कि 18 जुलाई 2012 जैसी हिंसा फिर कभी न हो।
इस ज्योतिषी के अनुसार, समस्या की जड़ यह थी कि इस फैक्ट्री की 600 एकड़ भूमि का एक हिस्सा कभी कब्रगाह हुआ करता था। इसके अलावा, उन्होंने कहा, संयंत्र स्थापित करने के लिए साइट पर मौजूद तीन मंदिरों को तोड़ दिया गया था। स्थल पर बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा थी। ज्योतिषी को दो से तीन सप्ताह तक चलने वाले अनुष्ठानों की एक शृंखला के माध्यम से साइट की सभी नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए कहा गया था।
यदि प्रबंधन भारतीय वैदिक ज्योतिष की प्रभावकारिता में विश्वास करता था, तो उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए था कि कर्मचारी ऐसी शक्तियों के असर में थे, जो उनके नियंत्रण से परे थी और उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए थे।
मारुति सुज़ुकी प्रबंधन भारतीय श्रम संहिताओं और श्रम क़ानूनों का लगातार उल्लंघन करता रहा है। वर्षों से वे स्थायी श्रमिकों को बाहर निकाल रहे हैं और केवल 18 से 26 वर्ष की आयु के श्रमिकों को रोज़गार दे रहे हैं – और वह भी केवल अस्थायी आधार पर।
बेरोज़गारी की चिंताओं और अनिश्चितताओं में भारत सरकार का स्किल इंडिया या कौशल भारत कार्यक्रम भी शामिल है, जिसने लगभग 30 करोड़ नौकरियाँ पैदा करने का वादा किया था। मारुति सुज़ुकी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किये जाने वाले मजदूरों को दो साल के लिए लिया जाता है, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें बिना कोई कौशल सिखाये असेंबली लाइन पर खड़ा कर दिया जाता है। उनसे स्थायी कर्मचारी की तरह ही काम कराया जाता है, लेकिन ऐसे वेतन पर, जो बमुश्किल न्यूनतम वैधानिक वेतन होता है।
मारुति सुज़ुकी के किसी भी प्लांट में काम कर चुके गैर-स्थायी कर्मचारियों ने हाल ही में 5 जनवरी, 2025 को एक यूनियन बनायी है। उन्होंने अपना माँग-पत्र श्रमायुक्त को दिया है। इन 5,000 पूर्व अस्थायी कर्मचारियों में से अधिकांश के लिए यूनियन ही एकमात्र आशा है। लेकिन उन्हें पुलिस लगातार परेशान कर रही है, दो अलग-अलग दिन उन्हें पूरा-पूरा दिन हिरासत में रखा गया और रात में रिहा किया गया।
जहाँ मारुति सुज़ुकी कंपनी सबसे बड़े साहित्यिक महाकुंभ को प्रायोजित कर रही है, कर्मचारियों और पूर्व-कर्मचारियों को एहसास हो रहा है कि उनका कोई भविष्य नहीं है। सरकार ने नयी श्रम संहिता लागू करने के अपने फ़ैसले की घोषणा की है, जिसमें निश्चित अवधि के रोज़गार को वैधता मिली है। प्रबंधन ने श्रमायुक्त से कहा है कि नयी यूनियन को वह मान्यता नहीं देता।
जयपुर लिटरेचर फ़ेस्टिवल में आने वाले हज़ारों आम लोग शायद नहीं जानते कि मारुति सुज़ुकी जैसी कंपनी भारतीय नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने में क्या भूमिका निभा रही है। मज़दूरों का दर्द साहित्यिक महाकुंभ में अदृश्य है।
भारत में, जिस तरह से निजी पूँजी न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति पर, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी असंगत प्रभाव डाल रही है, उसकी बहुत आलोचना नहीं हुई है। अंबानी और अडानी जैसे व्यक्तियों को निशाना बनाकर, हमने अन्य कॉरपोरेट्स की भूमिका को अदृश्य बना दिया है।
मारुति सुज़ुकी (और वेदांता) द्वारा जयपुर लिटरेचर फ़ेस्टिवल का प्रायोजन कॉर्पोरेट उदारता का एक मासूम कार्य नहीं है, बल्कि लेखकों, साहित्य, कविता और संस्कृति की क्रांतिकारी संभावनाओं को नियंत्रित करने की और उसके अन्तर्ध्वंस की कोशिश है। आज न सिर्फ़ इस तरह के प्रायोजन के ख़तरों को उजागर करने की ज़रूरत है, बल्कि लोगों की पीड़ाओं को सामने लाने और संस्कृति के क्षेत्र में उनके संघर्षों को प्रासंगिक बनाने के लिए इन मंचों का उपयोग करने की भी ज़रूरत है।

(लेखिका सुप्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार और प्रचारक हैं। साभार : नया पथ)